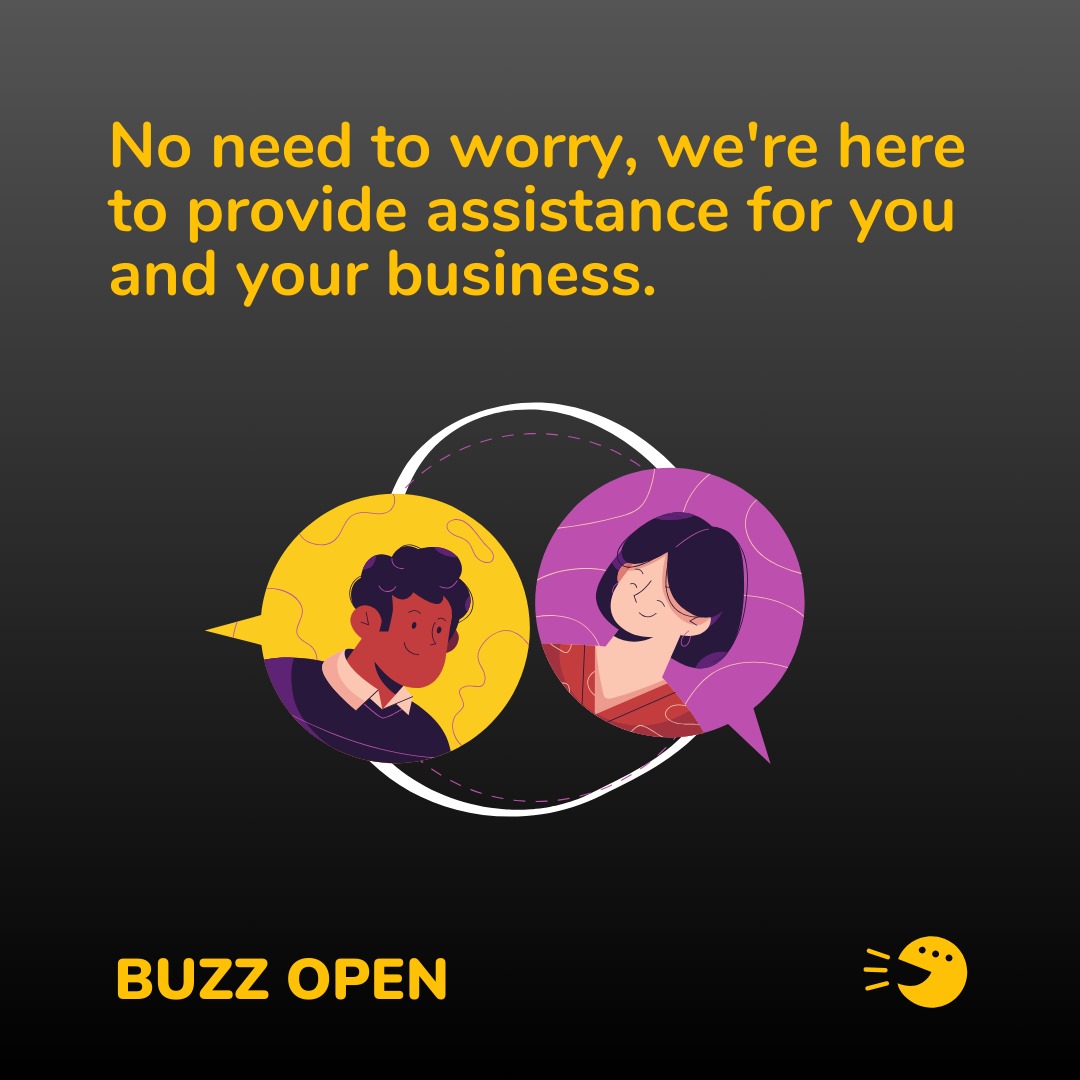उत्तराखंड का केदारनाथ धाम न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां के ऊंचे-ऊंचे पर्वत, हिमनद (ग्लेशियर) और बर्फीली चोटियाँ हजारों सालों से गंगा-यमुना जैसी महान नदियों के स्रोत रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केदारनाथ क्षेत्र और आसपास लगातार ग्लेशियर टूटने की घटनाएँ देखने को मिल रही हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है।
हाल की घटनाएँ
पिछले साल भी कई बार केदारनाथ के पीछे स्थित ग्लेशियरों के टूटने की घटनाएँ दर्ज की गईं। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की चिंता को और बढ़ा दिया है। ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और जलस्रोतों में असामान्य बढ़ोतरी होती है। इससे न केवल प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है बल्कि स्थानीय निवासियों और यात्रियों की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा हो जाता है।
पर्यावरणविद् और “ग्रीन मैन ऑफ यूपी” के नाम से विख्यात प्रदीप डाहलिया ने इस समस्या को बेहद गंभीर चिंता का विषय बताया है। उनका कहना है कि ग्लेशियर का बार-बार टूटना संकेत है कि हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन की सीधी चपेट में है।
यह केवल उत्तराखंड या भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है।
यदि ग्लोबल वार्मिंग और मानवजनित गतिविधियों पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में गंगा और अन्य हिमालयी नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।
प्रदीप डाहलिया पिछले 15 साल से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अब तक पाँच लाख से अधिक पौधे लगाए हैं और दिल्ली- एनसीआर के कई सूख चुके तालाबों को पुनर्जीवित किया है। उनका अनुभव बताता है कि यदि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ऐसी आपदाएँ और बढ़ेंगी।

ग्लेशियर टूटने के कारण
1. जलवायु परिवर्तन – ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी क्षेत्र में बर्फ तेजी से पिघल रही है।
2. अत्यधिक निर्माण कार्य – केदारनाथ और आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर हो रहे अनियंत्रित निर्माण कार्य प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं।
3. वनों की कटाई – वनों के घटने से जलवायु पर सीधा असर पड़ा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और मिट्टी का कटाव तेज हुआ है।
4. कार्बन उत्सर्जन – बढ़ते वाहनों, उद्योगों और मानव गतिविधियों से वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ी है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।
5. भू-वैज्ञानिक कारण – हिमालय अभी भी भूगर्भीय रूप से युवा पर्वत श्रृंखला है, इसलिए यहां भूमि खिसकने और ग्लेशियर टूटने की संभावना अधिक रहती है।
अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से मानव जीवन और बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान।
गंगा, यमुना जैसी नदियों में जलस्तर का असामान्य उतार-चढ़ाव।
कृषि, सिंचाई और पीने के पानी की गंभीर समस्या।
हिमालयी जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव।
तीर्थयात्रा और पर्यटन उद्योग पर संकट।
समाधान और सुझाव
प्रदीप डाहलिया जैसे पर्यावरणविदों का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, समाज और व्यक्तियों को मिलकर कदम उठाने होंगे। इसके लिए –
1. वनारोपण और तालाब संरक्षण – अधिक से अधिक वृक्षारोपण और पारंपरिक जलस्रोतों का संरक्षण जरूरी है।
2. पर्यावरणीय नियमों का पालन – निर्माण कार्यों और पर्यटन गतिविधियों पर सख्त पर्यावरणीय नियम लागू किए जाएं।
3. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा – सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाकर कार्बन उत्सर्जन घटाना होगा।
4. स्थानीय समुदाय की भागीदारी – स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में शामिल करना चाहिए।
5. वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी – ग्लेशियरों पर लगातार वैज्ञानिक अध्ययन और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
निष्कर्ष
केदारनाथ के पीछे बार-बार ग्लेशियर टूटने की घटनाएँ हमें यह बताती हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कितनी भारी पड़ सकती है। यह केवल उत्तराखंड की समस्या नहीं है बल्कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। पर्यावरणविद प्रदीप डाहलिया का कहना बिल्कुल सही है कि यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमें प्रकृति को बचाना ही होगा, तभी भविष्य सुरक्षित होगा।